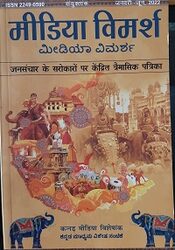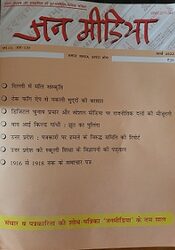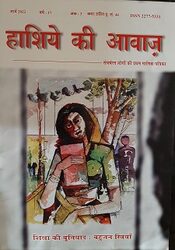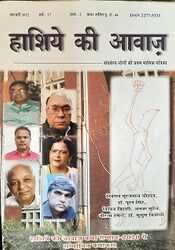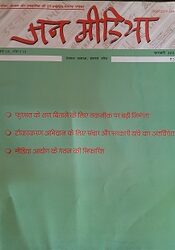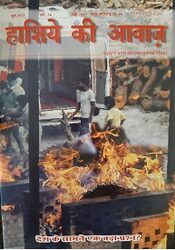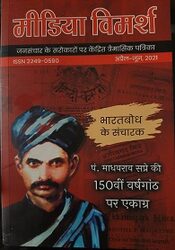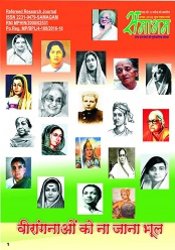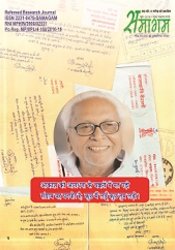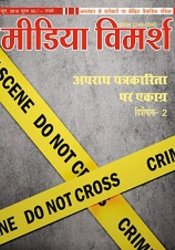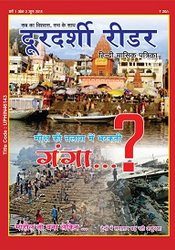मनोज कुमार/ मन आज व्याकुल है। ऐसा लग रहा है कि एक बुर्जुग का साया मेरे सिर से उठ गया है। मेरे जीवन में दो लोग हैं। एक दादा बैरागी और एक मेरे घर से जिनका नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूंगा। दोनों की विशेषता यह है कि उनसे मेरा संवाद नहीं होता है लेकिन वे मेरे साथ खड़े होते हैं। उनका होना ही मेरी ताकत है। दादा के जाने के बाद यह ताकत आधी हो गई है। दादा तो गाहे-बगाहे सलाह देते थे, डांट देते थे लेकिन अनकही ढंग से मेरी हौसलाअफजाई करते हैं। खैर, दादा के अचानक देवलोकगमन की खबर ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक था और लगभग नि:शब्द। अभी महीने भर पहले की तो बात है। ‘समागम’ का अंंक रेडियो पर केन्द्रित किया था। हर आलेख पर वे अपनी टिप्पणी से मुझे अवगत कराते रहे और बधाई देते रहे। कहते थे कि ऐसे समय में जब पत्रिकाओं की शताधिक संख्या है, उसमें श्रम करके जो प्रकाशन कर रहे हो, वह अतुलनीय है। मुझसे वे फोन पर जो बोलते थे, सो तो है। वे अपने अनन्य मित्रों और पत्रकार साथियों को भी ‘समागम’ पढऩे के लिए प्रेरित किया करते थे। मई महीने की बात है, साल याद नहीं। इंदौर के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सरोज कुमार का मुझे फोन आया। वे कहने लगे यार ऐसी कौन सी पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हो जिसकी तारीफ बैरागीजी कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर में व्याख्यान देने जाने के पहले ‘समागम’ के कुछ अंकों का अध्ययन कर लूं। डॉ. सरोज कुमार को मैं नाम से जानता हूं लेकिन परिचय नहीं था। अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन फूल गया लेकिन ऊपर से कहा कि यह दादा का मुझ पर स्नेह है। मैं आपको कुछ अंक प्रेषित कर रहा हूं, शायद उपयोगी हो। इसके बाद डॉ. सरोज कुमार से संवाद नहीं हुआ। संभव है कि ‘समागम’ को लेकर उनमें उतना उत्साह नहीं रहा होगा जितना कि दादा में था। बहरहाल, एक दिन दादा का फोन आया। तब मैंने साथी राजेश बादल की पत्रकारिता के संदर्भ में एक लम्बा साक्षात्कार प्रकाशित किया था। इसे वे राजस्थान की किसी पत्रिका में पुर्नप्रकाशन के लिए देना चाहते थे और मुझसे अनुमति चाह रहे थे। इन सालों में दादा से मेरा रिश्ता गहरा चुका था। कई बार लडक़पन में मैं उनसे दादागिरी किया करता था। अपनी सीमा लांघकर उनसे बातेें करने लगता था। मैंने जवाब में कहा कि आप भी कमाल करते हैं। आप जिसे चाहें, जो सामग्री चाहें,उपयोग करने के लिए भेज सकते हैं। इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत? लेकिन दादा तो दादा ठहरे। कहने लगे कि सम्पादक की अनुमति जरूरी होती है। एक बार फिर मैं उनका कायल ही नहीं हुआ बल्कि एक पाठ भी सीखा कि किसी का लिखा प्रकाशन करें लेकिन लेखक की अनुमति जरूर लें।
मनोज कुमार/ मन आज व्याकुल है। ऐसा लग रहा है कि एक बुर्जुग का साया मेरे सिर से उठ गया है। मेरे जीवन में दो लोग हैं। एक दादा बैरागी और एक मेरे घर से जिनका नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूंगा। दोनों की विशेषता यह है कि उनसे मेरा संवाद नहीं होता है लेकिन वे मेरे साथ खड़े होते हैं। उनका होना ही मेरी ताकत है। दादा के जाने के बाद यह ताकत आधी हो गई है। दादा तो गाहे-बगाहे सलाह देते थे, डांट देते थे लेकिन अनकही ढंग से मेरी हौसलाअफजाई करते हैं। खैर, दादा के अचानक देवलोकगमन की खबर ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक था और लगभग नि:शब्द। अभी महीने भर पहले की तो बात है। ‘समागम’ का अंंक रेडियो पर केन्द्रित किया था। हर आलेख पर वे अपनी टिप्पणी से मुझे अवगत कराते रहे और बधाई देते रहे। कहते थे कि ऐसे समय में जब पत्रिकाओं की शताधिक संख्या है, उसमें श्रम करके जो प्रकाशन कर रहे हो, वह अतुलनीय है। मुझसे वे फोन पर जो बोलते थे, सो तो है। वे अपने अनन्य मित्रों और पत्रकार साथियों को भी ‘समागम’ पढऩे के लिए प्रेरित किया करते थे। मई महीने की बात है, साल याद नहीं। इंदौर के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सरोज कुमार का मुझे फोन आया। वे कहने लगे यार ऐसी कौन सी पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हो जिसकी तारीफ बैरागीजी कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर में व्याख्यान देने जाने के पहले ‘समागम’ के कुछ अंकों का अध्ययन कर लूं। डॉ. सरोज कुमार को मैं नाम से जानता हूं लेकिन परिचय नहीं था। अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन फूल गया लेकिन ऊपर से कहा कि यह दादा का मुझ पर स्नेह है। मैं आपको कुछ अंक प्रेषित कर रहा हूं, शायद उपयोगी हो। इसके बाद डॉ. सरोज कुमार से संवाद नहीं हुआ। संभव है कि ‘समागम’ को लेकर उनमें उतना उत्साह नहीं रहा होगा जितना कि दादा में था। बहरहाल, एक दिन दादा का फोन आया। तब मैंने साथी राजेश बादल की पत्रकारिता के संदर्भ में एक लम्बा साक्षात्कार प्रकाशित किया था। इसे वे राजस्थान की किसी पत्रिका में पुर्नप्रकाशन के लिए देना चाहते थे और मुझसे अनुमति चाह रहे थे। इन सालों में दादा से मेरा रिश्ता गहरा चुका था। कई बार लडक़पन में मैं उनसे दादागिरी किया करता था। अपनी सीमा लांघकर उनसे बातेें करने लगता था। मैंने जवाब में कहा कि आप भी कमाल करते हैं। आप जिसे चाहें, जो सामग्री चाहें,उपयोग करने के लिए भेज सकते हैं। इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत? लेकिन दादा तो दादा ठहरे। कहने लगे कि सम्पादक की अनुमति जरूरी होती है। एक बार फिर मैं उनका कायल ही नहीं हुआ बल्कि एक पाठ भी सीखा कि किसी का लिखा प्रकाशन करें लेकिन लेखक की अनुमति जरूर लें।
‘समागम’ के प्रकाशन के इन 18 सालों में वे मेरे लिए गुरु और मार्गदर्शक के रूप में साथ रहे। कभी लगा नहीं कि वे मनासा में हैं और मैं भोपाल में बैठा हूं। हमेशा इस बात का अहसास रहा कि बस, उनका फोन आता ही होगा। इस संदर्भ में मुझे स्मरण में मराठी के एक कथाकार की वह लघुकथा जिसमें वे लिखते हैं कि एक बंद ताले को खोलने के लिए हथोड़े ने भारी-भरकम वार किया। हर तरह की कोशिश के बाद भी वह नाकामयाब रहा। इत्ते में पास पड़ी चाबी ताले के दिल में उतरी और ताला खुल गया। हथोड़ा अवाक और परेशान। उसने चाबी से अपनी ताकत और वजन की दुहाई देते हुए चाबी से पूछा कि तु इत्ती से फिर ताला कैसे खुल गया। मुस्कराती हुई चाबी ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि किसी का दिल खोलने के लिए उसके दिल में उतरा जरूरी होता है।
दादा से मेरा रिश्ता भी इसी ताला चाबी का था। मैं कब उनके दिल में उतर गया और कब उन्होंने मेरे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया, पता ही नहीं चला। बात दो-तीन साल पुरानी है। भोपाल के होटल अशोका में वे ठहरे थे। उन्हें मध्यप्रदेश शासन की ओर से कवि प्रदीप सम्मान दिया जाना था। मैं उनसे मिलने गया। अपने दर्द को भीतर ही भीतर रखते थे और समाज में आनंद को वे बेपनाह बांटते थे। लेकिन उस दिन वे अपना दिल खोल बैठे। बचपन से अब तक के अनुभवों को उन्होंने मुझसे शेयर किया। बचपन के कष्ट से लेकर आज तक की बातें बताते हुए उनकी पलकें कई बार भींग गई। हमेशा कडक़ आवाज में बात करने वाले दादा बैरागी का गला भर आया था। वे कहने लगे-‘आज ईश्वर का दिया हुआ सबकुछ है। लेकिन मैं आज भी कपड़े मांगकर पहनता हूं। यह इसलिए कि मैं अपने पुराने दिन भूल ना जाऊं।’
जब किसी का दिल खुलता है तो बस खुलता ही चला जाता है, यह मैंने पहली बार महसूस किया। पिता के शारीरिक परेशानियां, मां का दर्द, स्वयं भीख मांगकर गुजारा करने को कष्टप्रद अनुभव था, वह सिलसिले से शेयर करते गए। बात करते करते अचानक बीते दिनों से बाहर आए। चुपके से आंखों के आंसुओं को पोंछा और ठहाके लगा पड़े। कहने लगे-‘कई बार जिस मंच पर मैं उपस्थित होता हूं, उसी मंच से कोई नया या पुराना कवि मेरी ही कविता को अपने नाम से पढ़ता है। मैं मुस्करा कर रह जाता हूं, बल्कि आनंद भी प्राप्त करता हूं।’ वे आगे कहते हैं-‘मनोज, जब तक हम लिखते हैं, तब तक ही वह हमारी प्रापर्टी है। लिखने के बाद छपने के साथ ही वह समाज की हो जाती है। इसमें कोई कॉपीराइट जैसी बात नहीं होती है। तुम ऐसा ही करते रहना।’
बालकवि बैरागी ही उनका प्रचलित नाम हो चला था। वास्तव में उनका नाम नंदरामदास बैरागी था। वे बताते थे कि इस नाम से एक कविता तब की नईदुनिया में प्रकाशित हुई थी। इस कविता को जब एक लडक़ी ने पढ़ा तो वह अपने पिता से जिद कर नंदरामदास बैरागी से ब्याह करने अड़ गई। बाद में वही उनकी जीवनसंगिनी बनीं। शीर्ष पंक्ति के कवि और राजनीति के शीर्ष पर रहने वाले दादा बैरागी पूरा जीवन यूं ही बने रहे। अपने से छोटा किसी को माना नहीं और स्वयं को बड़ा होने दिया नहीं। वे साहित्य, राजनीति और पत्रकारिता के त्रयी थे लेकिन वर्तमान हालात से वे दुखी भी रहते थे लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन बदलेगा। अंधेरा छंटेगा और समाज में रोशनी आएगी। वे खरे थे और हमेशा खरे रहेंगे क्योंकि वे निर्दोष राजनेता थे और प्रतिबद्ध रचनाकार। हां, दुख इस बात का है कि साहित्य, राजनीति और पत्रकारिता का एक सूर्य अस्त हो गया है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं रिसर्च जर्नल ‘समागम’ के सम्पादक हैं) मोबा 9300469918