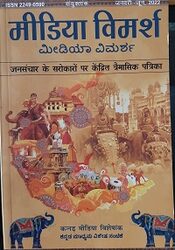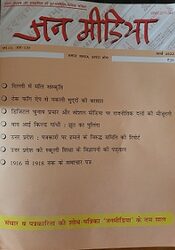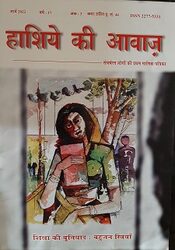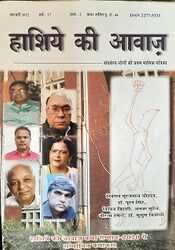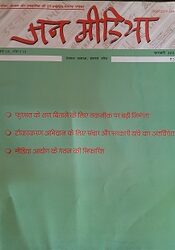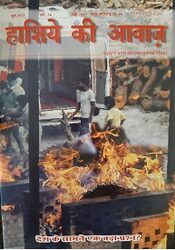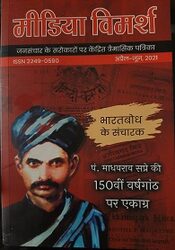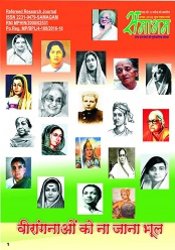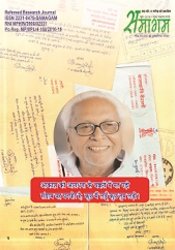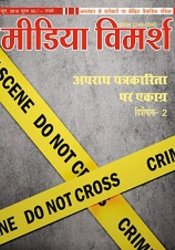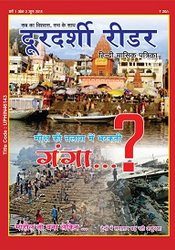जरा घड़ी भर ठहरकर यह सोच लें कि जब आपकी दिमागी खुराक सेठ प्रजाति के लोग तय करें तो उस खुराक में जहरीले तत्वों की मात्रा कितनी होगी?
जरा घड़ी भर ठहरकर यह सोच लें कि जब आपकी दिमागी खुराक सेठ प्रजाति के लोग तय करें तो उस खुराक में जहरीले तत्वों की मात्रा कितनी होगी?
दिनेश चौधरी। अखबार के दफ्तर में आने के बाद अखबार को लेकर जो कुछ भी आकर्षण, मोह, खिंचाव वगैरह रहा होगा; सब एक झटके में खत्म हो गया था। मेरे मन में अखबार की जो कल्पना थी और जो वह हकीकतन था, दोनों में जमीन-आसमान का अंतर था। इतने नीरस तो सरकारी महकमे भी नहीं हुआ करते। सम्पादक-उप सम्पादक-प्रशिक्षुओं की गर्दनें आम-तौर पर डेस्क पर ही झुकी रहतीं। हर वक्त कर्फ्यू-सा सन्नाटा छाया रहता, मानों यह एलान कर दिया गया हो कि किसी ने सिर उठाकर हँसने-बोलने की जुर्रत की तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। अमूमन अखबार के दफ्तरों में मिलने-जुलने वालों का तांता लगा होता है, पर लगता था कि उन्हें भी यहाँ हमेशा तारी कर्फ्यू के साये की थोड़ी-बहुत वाक़िफियत थी और वे बहुत जरूरी होने पर ही इधर का रुख करते थे। घड़ी के टिकटिक करने की आवाज भी साफ सुनाई पड़ती थी, पर इस अखबार का जिक्र मैं जरा आगे चलकर करूँगा। फिलहाल तो घड़ी की सुई यहाँ पर जरा उल्टी दिशा में घुमा ली जाए!
घर में जो अखबार आता था वह 'देशबन्धु' था। तब ब्लॉक वाली छपाई होती थी और अखबार मोनोक्रोम ही होते थे। छपाई को लेकर मेरे मन में हमेशा एक उत्सुकता रही है और अब भी प्रेस में जाने पर मैं धड़ाधड़ छपकर निकलते पन्नों को बड़े मनोयोग से देखता हूँ। स्याही की गंध मुझ पर जैसे नशा करने लगती है। ताजे निकले पन्नों को बड़े करीने से छूता हूँ और कोई इन्हें उल्टा-सीधा मोड़ दे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। प्रिंटिंग की तकनीकों को जानने-समझने में हमेशा मेरी गहरी दिलचस्पी रही। उन दिनों जब फ़ोटो कम्पोजिंग वाली तकनीक बहुत अधिक चलन में नहीं आई थी हम हाथ से बटर पेपर तैयार कर स्क्रीन प्रिंटिंग से यूनियन का बुलेटिन तैयार करने पर हाथ आजमा चुके थे। 'देशबन्धु' बड़ा अपना-सा लगता था। घर में अखबार को को पहले झपटने की होड़-सी रहती। पत्रकारिता में किए जाने अभिनव प्रयोगों का माद्दा तब इसी अखबार में था। नवभारत नम्बर एक था पर अपनी फितरत ऐसी रही कि अपन कभी उनके साथ नहीं रहे जो आगे हों। विश्वकप फुटबॉल में अपन जिस टीम के साथ होते हैं, वह हार जाती है। अपनी पसंद की फ़िल्म पिट जाती है। चुनाव में अपना केंडिडेट हार जाता है। यह अपने साथ बार-बार होता है और अब एक तरह से इसकी आदत पड़ गयी है। तो 'देशबन्धु' नम्बर दो होने के बावजूद अपना पसंदीदा अखबार था और यह जो उल्टा-सीधा अपन लिख पा रहे हैं, इसी के द्वारा डाले गए 'कुसंस्कारों' का नतीजा है। अपने साथ के लोग बड़े-बड़े पदों पर जाकर तबीयत से पैसे पीट रहे हैं और अपन ने कलम-घसीटी कर जितने कागद कारे किए उन्हें रद्दी के भाव बेचकर एक वक्त की रोटी नहीं जुटाई जा सकती!
अखबार में सबसे पसंदीदा कॉलम परसाई जी का 'पूछिए परसाई से' था। तब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी पर परसाई जी के पास पता नहीं कौन-सा गूगल था कि वे कठिन से कठिन सवाल का जवाब ढूँढ लाते। जवाब जितने ज्ञानवर्धक होते, उतने ही रोचक भी। अक्सर मजेदार। उनके व्यंग्य-आलेख भी पढ़ने को मिलते। लघु उपन्यास 'रानी नागफनी की कहानी' इसी में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। मुझे याद पड़ता है कि अस्तभान और मुफतलाल के कारनामों की कटिंग निकालकर हमने एक फाइल बना ली थी और जब कभी मन होता मजे लेकर उसका वाचन किया जाता। व्यंग्य की यह छाप अखबार के अन्य कॉलमों में भी दिखाई पड़ती। 'रायपुर डायरी' में मजेदार टिप्पणियां होतीं। घूरों की गंदगी पर एक बार लिखा गया कि अगर कैमरों में कैद होकर बदबू स्क्रीन में फैल पाती तो रामसे ब्रदर्स अपने फिल्मों की शूटिंग रायपुर में ही करते।
एक अन्य स्तम्भ जो बेहद लोकप्रिय था, 'घूमता हुआ आईना' था। इसके साथ छपने वाले स्केच की छवि बिल्कुल मेरी नजरों के आगे है और इसे कैप्चर करने की कोई तकनीक होती तो अभी यहीं पर आपके साथ साझा कर लेता। प्रभाकर चौबे गजब के जीवट वाले लिख्खाड़ हैं। जब अपन पढ़ रहे थे, जब मेट्रिक किया, जब कॉलेज गए, जब नौकरी पर आए, जब नौकरी से पिंड छुड़ा लिया; वे तब भी लिख रहे थे और अब भी लिख रहे हैं। मुझे कभी-कभी शुबहा होता है कि वे लेखक नहीं हैं, बल्कि एक लंबी मैराथन के धावक हैं, जो बस दौड़ता ही जाता है।
एस. अहमद और अनिल कामड़े के श्वेत-श्याम चित्र खासतौर पर आकर्षित करने वाले होते थे। इन चित्रों में पता नहीं ऐसी क्या बात होती थी कि वे आज के रंगीन चित्रों से भी ज्यादा सहज और जीवन के करीब लगते थे। मुझे लगता है कि उन चित्रों से एक खास आवृत्ति की तरंगें उठती रही होंगी, जिनमें दर्शक के दिलो-दिमाग को छू लेने वाली सलाहियत होती होगी। दरकती हुई जमीन के साथ शून्य में तकता किसान और खूँटे में बंधे बैल के साथ 'खेत सूखे और हम खाली' कैप्शन वाले चित्र की याद मुझे अब भी बेचैन करती है। तब से अब तक खेती-किसानी में कुछ भी तो नहीं बदला। इन 'ब्लैक एंड व्हाईट' तस्वीरों का नशा तब और भी गाढ़ा हो गया जब 'इंडिया टुडे' में रघु राय की शास्त्रीय संगीत के उस्तादों पर आधारित श्रृंखला देखी। यह पत्रिका मुझे कभी नही पसन्द नहीं आई क्योंकि इसका शुरू से एक एजेण्डा रहा है। जो काम इसका चैनल आज कर रहा है, यह पत्रिका वह काम शुरुआत से कर रही थी। यह बाजार के इशारों पर खेलने वाली पत्रिका, जिसके कुछ अंक मैंने सिर्फ रघु राय की वजह से खरीदे। और रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा कर देने वाली भोपाल गैस काँड वाली उस तस्वीर को भला कोई भूल सकता है!!
अखबार में हैडिंग बहुत सोच-समझ कर लगाई जाती थी। आजकल यह सिर्फ अंग्रेजी अखबार 'द टेलीग्राफ' में दिखाई पड़ता है। संजय गांधी का विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया था। देशबन्धु की फ्लैग हैडिंग मुझे अब तक याद है, " आज सिर्फ एक खबर।" लोकसभा को भंग कर आम चुनाव के ऐलान पर अखबार ने टेलीप्रिंटर के सन्देश का फोटो लेकर उसे शीर्षक का रूप दे दिया था , जो बेहद प्रभावी बन पड़ा था। गांव-गँवई की खबरें बस यहीं मिल पाती थीं। होली के दिन अखबार के खास तौर पर इंतज़ार होता। मालूम होता है कि 'फेक न्यूज' का चलन यहीं से शुरू हुआ होगा। भंग का नशा करने वाले अखबार को लेकर सातवें आसमान में उड़ने लगते। समझ में नहीं आता था कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी होली वाली!
'टाइम्स ऑफ इंडिया' के सौजन्य से आर.के. लक्ष्मण के कार्टून भी अखबार में देखने को मिल जाते थे। लक्ष्मण की पैनी निगाह से कोई क्षेत्र, कोई वर्ग अछूता नहीं रहता। उनका एक कार्टून याद आ रहा जिसमें हस्पताल में एक सज्जन की पतलून खिसकी हुई है और नितम्ब के एक छोर पर इंजेक्शन ठूँसा हुआ है। नर्स कह रही है, "मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। अगले शिफ्ट में आने वाली नर्स अब इसे बाहर निकालेगी।" एक अन्य कार्टून किसी सरकारी डिजाइनिंग विभाग का था। कुर्सी पर एक सज्जन उनींदे-से बैठे हैं। दीवार पर एक बिजली वाली केतली है। केतली से एक पाइप घूम-घाम कर कई मोड़ों के साथ चला आ रहा है। इसका दूसरा सिरा कुर्सी का हत्था है, जिस पर एक नलका लगा है और कुर्सी पर बैठे सज्जन इत्मीनान से इस नलके से चाय की प्याली भर रहे हैं। कैप्शन है, "ये जब से डिजाइनिंग विभाग में आए हैं, इन्होंने बस एक डिजाइन ही तैयार की है।" आर.के. लक्ष्मण शायद एक बार रायपुर भी आए थे और उनकी यात्रा पर 'देशबन्धु' में एक रपट की मुझे धुंधली-सी याद है। आगे चलकर उनके 'कॉमन मैन' पर आधारित एक सीरियल कुंदन शाह ने 'वागले की दुनिया' नाम से बनाई, जिसमें अंजन श्रीवास्तव ने मुख्य भूमिका निभाई और वे हर घर में जाने-पहचाने से हो गए। अब कभी-कभार वे इप्टा की मीटिंग में मिल जाते हैं तो दुआ-सलाम हो जाती है।
तब अखबार की कीमत 70 या 75 पैसे थी और यह 70 के दशक का अंतकाल रहा होगा। सिनेमा में थर्ड क्लास की टिकिट भी लगभग इतने ही पैसों में मिलती थी। एक दिन अखबार में एक टिप्पणी आई कि कागज के दाम निरन्तर बढ़ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब अखबार 1 रुपये का हो जाएगा। अखबार जब 1 रुपये का हो गया तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी अब होती है जब अखबार सिर्फ दो रुपये में मिल जाता है। इस मामले को इस तरह से समझें कि वर्ष 80 के बाद जब चीजों के दाम कई गुना बढ़ गए तो अखबार कोई दो-तीन गुने पर ही क्यों रुक गया? आकलन की यही प्रणाली खाद्यान की कीमतों पर भी आजमाएँ। हमारे घरेलू बजट में हम सबसे कम खर्च अपनी जिस्मानी खुराक के लिए कर रहे हैं। दिमागी खुराक के लिए उससे भी कम, बहुत कम। तो जो अखबार आज 2 रुपये में मिल रहे हैं, वे 2 रुपये के नहीं हैं और सच कहूँ तो 2 रुप्पइये के लायक भी नहीं हैं! इनकी लागत बहुत ज्यादा है पर बाकी का पैसा बड़े-बड़े सेठ दे रहे हैं। बस जरा घड़ी भर ठहरकर यह सोच लें कि जब आपकी दिमागी खुराक सेठ प्रजाति के लोग तय करें तो उस खुराक में जहरीले तत्वों की मात्रा कितनी होगी?
(क्रमशः)
(दिनेश जी के फेसबुक वाल से साभार)