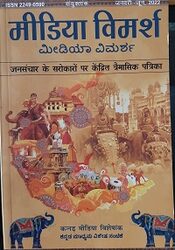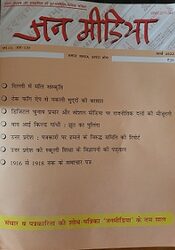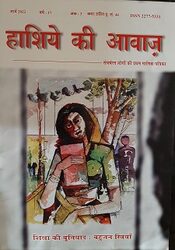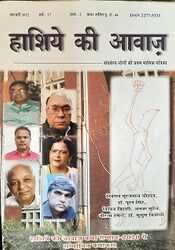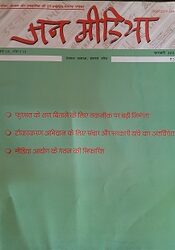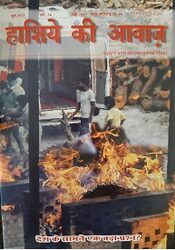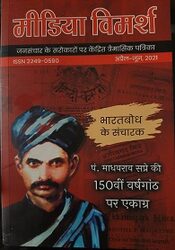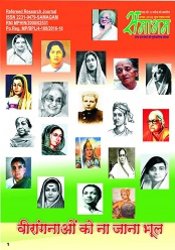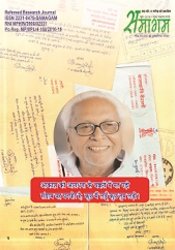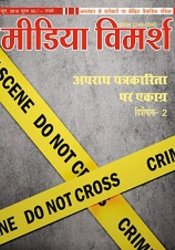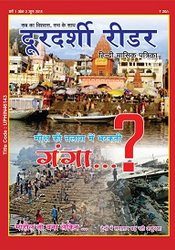संजय द्विवेदी/ उदारीकरण और भूमंडलीकरण की इस आँधी में जैसा मीडिया हमने बनाया है, उसमें ‘भारतीयता’ और ‘भारत’ की उपस्थिति कम होती जा रही है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में मीडिया का पारंपरिक चेहरा-मोहरा कहीं छिप सा गया है। वह सर्वव्यापी और सर्वग्रासी विस्तार लेता हुआ, अपने प्रभाव से आतंकित तो कर रहा है किंतु प्रभावित नहीं। आस्था तो छोड़िए उसके प्रति भरोसा भी कम हो रहा है। आक्रामकता, चीख-चिल्लाहट और वैचारिक विरोधियों के साथ शत्रुओं का व्यवहार इस मीडिया का नया सलीका है।
संजय द्विवेदी/ उदारीकरण और भूमंडलीकरण की इस आँधी में जैसा मीडिया हमने बनाया है, उसमें ‘भारतीयता’ और ‘भारत’ की उपस्थिति कम होती जा रही है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में मीडिया का पारंपरिक चेहरा-मोहरा कहीं छिप सा गया है। वह सर्वव्यापी और सर्वग्रासी विस्तार लेता हुआ, अपने प्रभाव से आतंकित तो कर रहा है किंतु प्रभावित नहीं। आस्था तो छोड़िए उसके प्रति भरोसा भी कम हो रहा है। आक्रामकता, चीख-चिल्लाहट और वैचारिक विरोधियों के साथ शत्रुओं का व्यवहार इस मीडिया का नया सलीका है।
ऐसा लगता है जैसे वैश्विक प्रवाह में बहते हमारे संचार माध्यमों ने आत्मसमर्पणकारी मुद्रा अख्तियार कर ली है। उनका खुद का सोच, चिंतन और अलग-अलग होना भी नहीं गुम हो रहा है। सारे अखबार, टीवी चैनल और मनोरंजन चैनल एक ही रूप और एक ही मुद्रा अख्तियार कर लें तो पाठक और दर्शक कहां जाएं, क्या करें। मीडिया की लोकजागरण और रूचि परिष्कार की महती जिम्मेदारी भी है। किंतु संचार माध्यम कह रहे हैं कि वे अपने ग्राहकों (पाठकों) जैसा होना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कुछ अलग-अलग सा दिखे। वे स्पर्धा से हलाकान हैं, टीआरपी से बेजार है। उनका आत्मविश्वास हिल गया लगता है। अच्छे और सच्चे का बाजार भी बन सकता इससे भरोसा गायब है। इसलिए आजमाई गयी चीजें दोहराई जा रही हैं। कहानियां बनाई जा रही हैं भले ही मैदान से उनका वास्ता न हो। मैदान में जाने और गंभीर खबरें करने का अभ्यास कम हो रहा है। जो कर रहे हैं वे विरले हैं और बहुत कम। सही मायने में आज का मीडिया ‘असली भारत’ के पास बहुत कम पहुंचता है। वह जमीन तक नहीं पहुंचता इसलिए देश की चमकीली प्रगति से आह्लादित और खासा प्रसन्न है। उसे नहीं पता कि देश कहां है और उसके लोग कहां बसते हैं। हमारा मीडिया लुटियंस की दिल्ली से शुरू होकर चार मेट्रो की परिक्रमा कर जिला कलेक्टरों की देहरी तक आकर दम तोड़ देता है। इसके नीचे ना तो वह जाना चाहता है न जाता है। ये भला हो पांच साल पर होने वाले चुनावों का जिसके चलते मीडिया के चमकते देवदूत भी भारत का कुछ हिस्सा देख लेते हैं, भले ही वे देश के बेचारे शहर क्यों न हों। यह संकट दिनों दिन गहरा हो रहा है। देश के राजनेताओं से जवाब मांगने वाला मीडिया खुद जड़ों से कटा है, वह राजनेताओं का हिसाब क्या लेगा। राजनीति की पथरीली जमीन और वास्तविक समाज से मीडिया की बढ़ती हुयी दूरी ने उसे सिर्फ प्रभुवर्गों की वाणी बना दिया है। मीडिया से जो समाज उद्भभूत हो रहे हैं उसमें राजकाज और बाजार की शक्तियां ही केंद्र में हैं। कुलीन समाज को दिखाते-बताते और सुनाते मीडिया खुद कुलीनों का प्रवक्ता बनता जा रहा है। जनता के दुख-दर्द, उसके सपने उसकी आंखों से लापता हैं। वह समाज को खास नजर से देखता है। संघर्ष में लगी जनता को वह हिकारत से देखता है। आम आदमी का इस्तेमाल वह जुमलों की तरह करता है पर उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखता। नए समय का मीडिया पाठकों की नहीं ग्राहकों की प्रतीक्षा में है। वह सताए हुए लोगों के साथ नहीं त्रास देने वाली शक्तियों के साथ खड़ा दिखता है। उसकी चिंता के केंद्र में समाज नहीं प्रभुवर्ग है। संपन्न लोग हैं। मीडिया ने मध्यवर्ग को ऐसे चमकीले सपनों में फंसा दिया है कि उसने भी मीडिया की तरह समाज से मुंह मोड़ लिया है। मीडिया और मध्यवर्ग के सपने कमोबेश एक ही हैं। दोनों ही एक सपनीली दुनिया में सफर कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके सपने ही शेष समाज के सपने बन जाएं। इन दोनों ने देश के सपनों, उसकी आकांक्षाओं और संघर्षों से मुंह मोड़ लिया है। सवाल यह उठता है किक्या भारतीय मीडिया वंचितों को मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता हुआ नजर आता है? क्या वह सामाजिक समरसता बढ़ाने की दिशा में सचेतन प्रयास करता दिखता है, क्या ऐसे कुछ उदाहरण हमारे पास हैं? 1990 के बाद की पत्रकारिता और मीडिया का स्वर पूरी तरह बदला हुआ दिखता है। उसके लिए खबरें नहीं स्टोरी महत्व की है। मीडिया के इस समय के नायकों ने अपने पाठकों-दर्शकों को एक अराजनैतिक समाज में बदलने के सचेतन प्रयास किए हैं। मुद्दों से भटकाव और देश की वास्तविकताओं से अलग एक नई तरह की दुनिया बनाने के प्रयास दिखते हैं। मीडिया की नीतियां कहां से तय हो रही हैं कहना मुश्किल है। संपादक वातावरण से अनुकूलन करने के प्रयासों में हैं। व्यक्तित्वहीन और चेहराविहीन नायकों ने बड़ी जगहें हथिया ली हैं। वे ही मुद्दे तय कर रहे हैं और निरर्थक व अंतहीन बहसें भी। उनकी इस बहस से चपलता में देश में सच कम फैलता है भ्रम ज्यादा। शायद इसीलिए मीडिया में राजकाज के द्वंद प्रमुखता पाते हैं न की राजकाज की विशेषताएं प्रमुखता पाती हैं?
इस प्रवृत्ति की तीखी आलोचना के बाद अखबारों ने सन 2000 के बाद अपना नया सामाजिक चेहरा बनाना प्रारंभ किया, जिसके तहत पर्यावरण, पानी, टाइगर बचाने, सूखी होली जैसे अभियान दिखते हैं। इसी तरह कारपोरेट सोशल रिस्पांस्बिलिटी(CSR) जैसे यत्न क्या कंपनियों के सोशल फेस बनाने जैसा नहीं है? लेकिन क्या ऐसे साधारण प्रयासों से मीडिया आम जनता का भरोसा पा सकता है। सामाजिक होने और सामाजिक दिखने का बहुत अंतर है। मीडिया ने जनता का भरोसा खोया है तो उसका कारण यही है कि उसने समाज की तरफ देखने की अपनी दृष्टि विकसित करने के बजाए उधार की नजरें ली हैं। उसने कारपोरेट सोशल रिस्पांस्बिलिटी की तरह अपना चेहरा बनाया है। जहां बहुत सी गतिविधियों में सामाजिक काम भी एक गतिविधि है। मीडिया की मूल गतिविधि समाज नहीं है, उसके सपने, संघर्ष और आकांक्षाएं नहीं हैं। यह देखना रोचक है कि मीडिया की यह आलोचना भी अब उसे सुनाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में भारत जैसे महादेश को उसकी विविधता और बहुलता के साथ व्यक्त करना एक कठिन चुनौती है। तमाम पत्रकार और मीडियाकर्मी इस विपरीत हवा में भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यह संख्या में कम हैं पर संकल्प के तेज से दमक रहे हैं। इस धारा को मजबूत करने की जरूरत है। यह अचरज की बात ही है कि जबकि ज्यादातर मीडियाकर्मी अपने काम के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध हैं तो मीडिया का चेहरा इतना विद्रूप क्यों है? जाहिर तौर पर मीडिया पर कम हुए सामाजिक नियंत्रण ने यह हालात पैदा किए हैं। हमने अपने मीडिया को कुछ ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ दिया है जो न मीडिया को समझते हैं न भारत को। इसलिए एक परिवर्तनकामी माध्यम को आर्थिक उद्यम में बदलनेवालों ने इसे विकृत कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि पाठक,दर्शक और श्रोता सब इस माध्यम पर सकारात्मक दबाव बनाएं और मीडिया को उसके वास्तविक धर्म की याद भी दिलाएं।
(लेखक मीडिया विमर्श पत्रिका के कार्यकारी संपादक और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं)