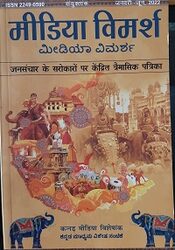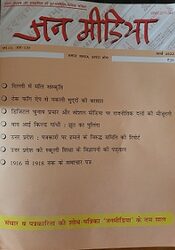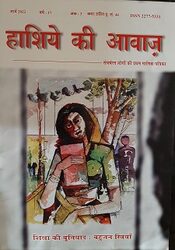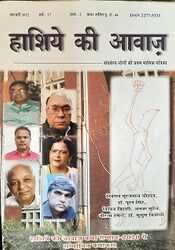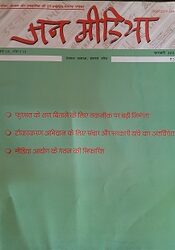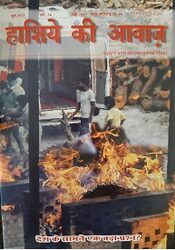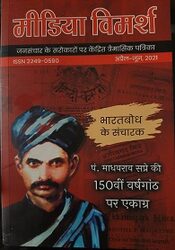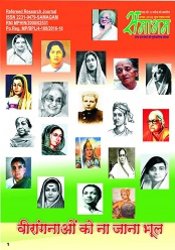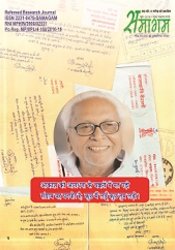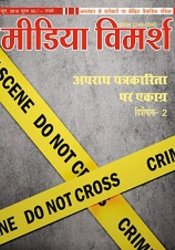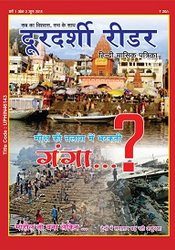मीडियाकर्मियों के लिए एबीपी समूह में व्यापक छंटनी भयंकर दुःसमय की सबसे बड़ी चेतावनी!
मीडियाकर्मियों के लिए एबीपी समूह में व्यापक छंटनी भयंकर दुःसमय की सबसे बड़ी चेतावनी!
पलाश विश्वास/ मीडियाकर्मी इसे अच्छी तरह समझ लें कि उनकी कार्यस्थितियों को नर्क बनाने से लेकर उनका सीआर खराब करने और उसी के आधार पर उन्हें काम से निकालने में मीडिया के मसीहा तबके की शैतानी भूमिका हमेशा निर्णायक होती है। कारपोरेट हितों के मुताबिक अपनी चमड़ी बचाने और जल्दी जल्दी सीढ़ियां छंलागने के लिए यह तबका किसी की भी बलि चढ़ाने से हिचकता नहीं है।
1991 से मीडिया में गैरपत्रकारों की छंटनी का विरोध, पत्रकारों ने कभी नहीं किया है और यूनियनों के नेतृत्व में रहे पत्रकारों ने सबसे पहले गैरपत्रकारों की कुर्बानी देकर आटोमेशन तेज किया है।
यह भोगा हुआ यथार्थ है कि यूनियनें मालिकान की पहल पर चुनिंदा पत्रकारों की अगुआई में ही बनीं, जिसने पत्रकारों और गैरपत्रकारों की बलि चढ़ाकर अपना कैरियर सवांरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के हालात के लिये यह क्रांतिकारी मसीहा तबका मालिकों से ज्यादा जिम्मेदार हैं। आगे मीडियाकर्मी ऐसी गलती न दुहरायें तो बेहतर।
इसी आटोमेशन के खिलाफ आवाज उठाने में मेरा अपने सीनियर साथियों से दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ी है। लेकिन हम अपने साथियों को बचाने में नाकाम रहे हैं। अब हम अनेक संपादकों और अपने पुराने सीनियर जूनियर साथियों के क्रांतिकारी तेवर से ज्यादा चकित हैं, जिन्होंने पेशेवर जिंदगी में हमेशा कारपोरेट हितों के मुताबिक बाजार के व्याकरण के मुताबिक पत्रकारिता की है और नौकरी में रहते हुए कारपोरेट लूट खसोट और जल जंगल जमीन के हकहकूक की आवाज उठाते जनपदों और जनसमूहों के उत्पीड़न सैन्य दमन से लेकर मेहनतकश तबकों के आंदोलन और बहुजनों पर सामंती अत्याचारों के खिलाफ बाकी मीडियाकर्मियों की तुलना में नीतिगत फैसलों की बेहतर स्थिति के बावजूद पिछले छब्बीस सालों में एक पंक्ति भी नहीं लिखी है और न अपने साथियों के हकहकूक के लिए कभी जुबान खोली है।
मीडिया का यह पाखंडी मसीहा तबका सत्तावर्ग ही बाकी मीडियाकर्मियों का सबसे बड़ा दुश्मन हैं। क्योंकि वे बाकायदा मीडिया प्रबंधन के हिस्सा बने रहे हैं। इन लोगों से सावधान रहने की जरुरत है।कारपोरेट हितों के लिए वे हमेशा पेरोल पर हैं।
हमने अपनी पेशेवर पत्रकारिता के 36 सालों में अपने साथियों को बचाने की हर संभव कोशिशें की हैं। जरुरत पड़ी तो किसी किसी पर हाथ भी उठाया है, लेकिन ऐन मौके पर उनकी गलतियों की जिम्मेदारी लेकर सजा भुगतने में और अपने कैरियर का बंटाधार करने में भी हिचकने की जरुरत महसूस नहीं की है। हमने किसी की शिकायत करने के बजाये हमेशा खुद हालात से निबटने की कोशिशें की हैं और जाहिर है कि मैनेजमेंट की आंखों में किरकिरी बने रहने में या उसे डराने में मुझे मजा आता रहा है।
हस्तक्षेप पर अरविंद घोष की रपट से सदमा जरुर लगा है, लेकिन हमारे लिए यह कोई अचरज की बात नहीं है। मीडिया में पेशेवर नौकरी में रहते हुए हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा है।
एबीपी समूह शुरु से ही मुक्तबाजार व्यवस्था का सबसे मुखर प्रवक्ता रहा है और इस मायने में टाइम्स समूह उसका देश में एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है।
दुनियाभर में ट्रंप समर्थक अमेरिकी फाक्स न्यूज के साथ उसकी तुलना की जा सकती है जो वर्चस्ववादी नस्ली रंगभेद के सत्तावर्ग की संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है।
टीवी 18 समूह और हिंदुस्तान समूह के रिलायंस के हवाले हो जाने के बाद मीडिया कर्मियों के लिए एबीपी समूह में व्यापक छंटनी भयंकर दुःसमय की सबसे बड़ी चेतावनी है। अरविंद ने लिखा हैः
Strongly condemn the retrenchment on 7th February, 2017 with only 2 hours notice, of about 750 workers, journalists and reporters of Ananda Bazar Patrika group of newspapers of Kolkata. Express solidarity with the retrenched workers and journalists and their affected families.
यह हालत अचानक नहीं बनी है।
मीडियाकर्मियों की जनपक्षधर चरित्र के लगातार हो रहे स्खलन और उनके आत्मघाती तरीके से मार्केटिंग और सत्ता की पैदल सेना बन जाने से समूचा मीडिया इस वक्त बारुदी सुंरगों से भरी मौत की घाटी में तब्दील है।
गैरपत्रकार तबकों की छंटनी का कभी विरोध न करने वाले पत्रकार अब मीडिया में गैरपत्रकारों के सारे काम मसलन कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग, लेआउट, फोटोशाप, पेजमेकिंग से लेकर विज्ञापनें लगाकर सीधे मशीन तक अखबार छापने के लिए तैयार, करने का काम करते हैं. जबकि 1991 से पहले इन सारे कामों के लिए अलग अलग विभाग गैरपत्रकारों के थे। आटोमेशन मुहिम के चलते एक एक करके वे सारे विभाग बंद होते चले गये। अखबारों में अब दो ही सेक्शन हैं, संपादकीय और प्रिंटिंग मशीन।
संपादकीय विभाग का काम भी मूल सेंटर के अलावा बाकी सैटेलाइट संस्करणों में इलेक्ट्रानिक इंजीनियर कर देते हैं। इसके खातिर पत्रकारों की संख्या बहुत तेजी से घटी है। प्रिंटिंग सेक्शन में भी बचे खुचे कर्मियों को अपने संस्थान के अखबारों के अलावा एक साथ दर्जन भर से ज्यादा अखबारों का काम संस्था के जाब वर्क बतौर काम के घंटों के अंदर अपने वेतनमान के अलावा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के करना होता है।
मीडिया संस्थानों में स्थाई नौकरी वाले पत्रकार- गैर पत्रकार विलुप्त प्राय हैं। जो हैं वे रिटायर करने वाले ही हैं। उन्हें आगे एक्सटेंशन मिलने की कोई संभावना नहीं है।
अगले पांच सालों में मीडिया में सारे कर्मचारी ठेके की नौकरी पर होंगे। आटोमेशन के सौजन्य से किसी की खास काबिलियत का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बाजार के मुताबिक छंटनी का यह सिलसिला चलने वाला है।
वेज बोर्ड से बचने के लिए देशभर में असंख्य संस्करण आटोमेशन के जरिये छापते रहने की वजह से मीडिया में कोई पत्रकार या गैरपत्रकार,चाहे उनकी काबिलियत या हैसियत कुछ भी हो, अपरिहार्य नहीं हैं, जैसे हम लोग 1991 से पहले हुआ करते थे। सिर्फ अपने काम और अपनी दक्षता के लिए उन दिनों पत्रकारों के सात खून माफ थे।
मीडिया ने मुझ जैसे बदतमीज पत्रकार को भी 36 साल तक झेल लिया और आजादी का चस्का लग जाने से मैंने भी 36 साल तक मीडिया को झेला। अब हमारे जैसे लोगों के लिए मीडिया में कोई जगह नहीं बची है।
इसलिए मीडिया में हर छोटे बड़े पत्रकार गैरपत्रकार के सर पर छंटनी की तलवार लटकी हुई है। आंखें बंद करके कारपोरेट या मार्केट के हित में कामा करते रहने की वफादारी से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जब प्रेतात्माओं से मीडिया का काम चल सकता है, तो मनुष्यों को मीडिया की कोई जरुरत नहीं है।
हम जब दैनिक जागरण में मुख्य उपसंपादक बतौर काम कर रहे थे,1984 और 1989 के दौरान, तब माननीय नरेंद्र मोहन समूह के प्रधान संपादक थे। संपादकीय विभाग के कामकाज में वे हस्तक्षेप नहीं करते थे।
संस्करण मैं ही निकालता था। ऐसा वक्त भी आया कि रातोंरात सारे पत्रकार भाग निकले और डेस्क के सामने सबएडीटर की कुर्सी पर सिर्फ नरेंद्रमोहन जी अकेले थे। उस वक्त नये पत्रकारों की भरती का विज्ञापन सबसे पहले तैयार करना होता था और आवेदन मिलते न मिलते उन्हें नियुक्ति देकर ट्रेनी पत्रकार बतौर उन्हें काम के लायक बनाना होता था।
विज्ञापन छापने से लेकर भर्ती और प्रशिक्षण मेरठ में मेरी जिम्मेदारी थी तो कानपुर में आदरणीय बीके शर्मा की और समूह के समाचार संपादक तब हरिनारायण निगम थे।
मुश्किल यह था कि छह सौ रुपल्ली से ज्यादा छात्रवृत्ति किसी को दी नहीं जाती थी। यह मरेठ की पगार थी। लखनऊ में तीन सौ रुपये की छात्रवृत्ति थी। खुराफात की वजह से जब उन्हीं तीन सौ रुपये की पगार पर उन्हें मेरठ स्थान्तरित कर दिया जाता था, हमारे लिए मानवीय संकट खड़ा हो जाता था।
सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि नरेंद्र मोहन जी का आदेश था कि स्टिक बाई स्टिक मापकर पांच कालम का अनुवाद और पांच कालम के संपादन का काम सबसे लेना है चाहे अखबार में कुल दस कालम की भी जगह न बची हो।
हम लगातार प्रशिक्षुओं को स्थाई बनाने पर जोर देते रहते थे और अक्सर ऐसा नहीं हो पाता था। काम सीखते ही एक साथ भर्ती तमाम प्रशिक्षु झुण्ड बनाकर कहीं भी, किसी भी अखबार में भाग निकलते थे क्योंकि तब जागरण ट्रेनिंग सेंटर से निकले पत्रकारों की बाजार में भारी मांग होती थी । स्थाई पत्रकार भी वेतन सात सौ आठ सौ रुपये से ज्यादा न होने की हालत में अक्सर निकल भागते थे।
फिर नये सिरे से भर्ती और प्रशिक्षण की कवायद। आदरणीय बीके शर्मा के बाद शायद मैने ही सबसे ज्यादा पत्रकारों को जागरण में नियुक्ति दी है और प्रशिक्षित किया है। इसलिए साथी पत्रकारों की नौकरी के आखिरी दिनों में भी मुझे बेहद परवाह होती थी।
प्रभात खबर, जागरण और अमरउजाला में हम कंप्यूटर पर बैठते नहीं थे। कंपोजीटर, प्रूफरीटर, पेजमेकर अलग थे। कैमरा और प्रोसिंसग के विभाग अलग थे। कोलकाता में आये तो लेआउट आर्टिस्ट भी दर्जनभर से ज्यादा थे।
बीके पाल एवेन्यू में दोनों अखबारों में सौ से ज्यादा पत्रकार थे और लगभग सभी स्थाई थे। इनके अलावा जनसत्ता के करीब डेढ़ सौ स्ट्रींगर थे। दस साल पहले भी ग्रांट लेन के आफिस में इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत पर सौ से ज्यादा पत्रकार थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आटोमेशन सबसे पहले हुआ। फिर जनसत्ता का।
आटोमेशन ने सारी भीड़ छांट दी।
अब जनसत्ता कोलकाता में मेरे और शैलेंद्र के रिटायर होने के बाद स्थाई पत्रकार सिर्फ दो डा.मांधाता सिंह और जयनारायण प्रसाद रह गये तो एकमात्र स्टाफ रिपोर्टर प्रभाकरमणि तिवारी। बाकी दो अखबारों में एक भी स्थाई पत्रकार नहीं हैं।
आफिस और मार्केटिंग में मैनेजर भी सारे के सारे ठेके पर हैं। दो आर्टिस्ट सुमितगुहा और विमान बचे हैं स्थाई। कंपोजिग के पुराने साथियों में प्रमोद कुमार और संपादकीय सहयोगी महेंद्र राय स्थाई हैं जो मार्केटंग के लिए काम करते हैं।
मशीन में पुराने कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे ठेके पर हैं।
यह किस्सा हकीकत की जमीन पर कयामती फिजां की तस्वीर है।
एबीपी भाषाई अखबार समूह है ,जहां आटोमेशन शायद सबसे पहले शुरु हुआ। लेकिन बांग्ला में इंटरनेट से हिंदी और अंग्रेजी की तरह सारा कांटेट रेडीमेड लेने की स्थिति न होने और करीब पंद्रह करोड़ बांग्ला पाठकों की वजह से उन्हीं मौलिक कांटेंट की जरुरत पड़ती है। इसलिए आटोमेशन और ठेके की नौकरी के बावजूद वहां पत्रकारों- गैरपत्रकारों की फौज बनी हुई थी।
यानी बांग्ला और दूसरी भारतीय भाषाओं के मीडिया में भी हिंदी और अंग्रेजी की तरह प्रेतात्माओं से अब काम लिया जाना है। प्रेतात्माओं का वर्चस्व मनुष्यों के वजूद को खत्म करने वाला है। इंसानियत का जज्बा खतम है तो जाहिर है कि अब सिर्फ मशीनें बोलेंगी। अभी रोबाट आया नहीं है और यह हाल है. आगे क्या होगा, मीडियाकर्मी सोच समझ लें तो बेहतर।
जाहिर है कि आटोमेशन, मशीनीकरण, आधुनिकीकरण, उपभोक्तावाद और मुक्तबाजार का पत्रकारों ने जिस अंधेपन से समर्थन किया है, उससे सत्तावर्ग और मुक्तबाजारी राजनीति के नरसंहारी अश्वमेधी अभियान में चुनिंदा मौकापरस्त पत्रकारों के राजनीति, सत्ता और यहां तक कि पूंजीवादी तबक में एडजस्ट होने की कीमत अब मीडियाकर्मियों को हर हालत में चुकानी होगी।
साथियों की निरंतर छंटनी का प्रतिरोध पत्रकार जमात ने चूंकि कभी नहीं किया है और छंटनी का सिलसिला पत्रकारों के सहयोग से निर्विरोध जारी रहने की वजह से यूनियन बनाकर लड़ने की संख्या और ताकत भी उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ श्रम कानून सिरे से खत्म हो जाने पर ऐसी लड़ाई से भी अब पायदा नहीं है। वेज बोर्ड का किस्सा काफी है प्रेस और मीडिया में कानून के राज का सच बताने के लिए।
हाल में भड़ास के मजीठिया मंच से कानूनी लड़ाई का एकमोर्चा जरूर खुला है लेकिन मीडिया में इस वक्त संपूर्ण आटोमेशन होने की वजह से वेतनमान की लड़ाई भले आप लड़ लें, तेज होती छंटनी रोकने का आसार बेहद कम है।
अब मीडियाकर्मियों को फर्जी मसीहा वर्ग की प्रेतात्माओं के शिकंजे से बाहर निकालकर अपनी जनमुखी भूमिका में वापस आने का सही वक्त है क्योंकि अब खोनेका कुछ भी नहीं है। हमने यह फैसला 1991 में ही कर लिया था।
सिर्फ तरक्की और प्रोमोशन के मौके के अलावा मैंने कुछ नहीं खोया है। अब रिटायर होने के बाद भी बाकायदा जिंदा हूं और अपने मोर्चे पर अडिग हूं।
जीवित मृत मसीहा संप्रदाय से मेरी स्थिति बेहतर है क्योंकि मैंने पाखंड जिया नहीं है और आम जनता के साथ सड़क पर खड़े होने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरी नियति तो अपने पुरखों की तरह अपने गांव खेत खलिहान में किसी आपदा में मर जाने की थी। पढ़ लिखकर मैं अपने लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटा सका और पत्रकरिता को उनके हक हकूक की लड़ाई के हथियार बतौर इस्तेमाल करने की हमेशा कोशिश की, मरते वक्त कम स कम मुझे मामूली पत्रकार होने का अफसोस नहीं होगा। चाहे हासिल कुछ नहीं हुआ हो।
मेरे पत्रकार मित्रों,पानी सर से ऊपर है और पांव तले जमीन भी खिसक रही है। बतौर पत्रकार जनता के साथ खड़े होने का इससे बेहतर मौका नहीं है।