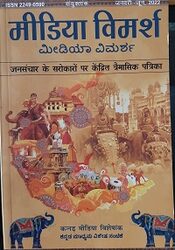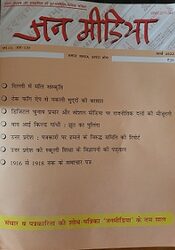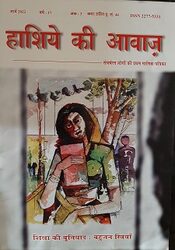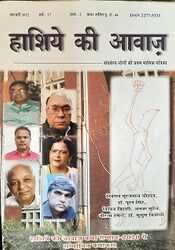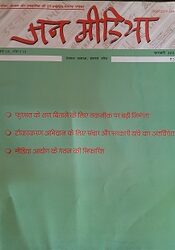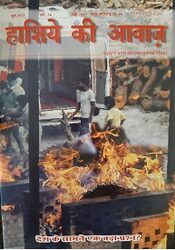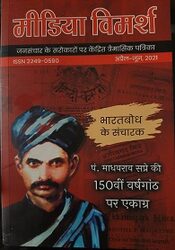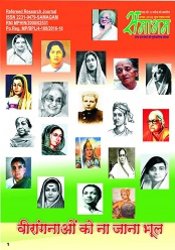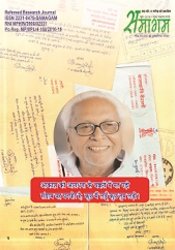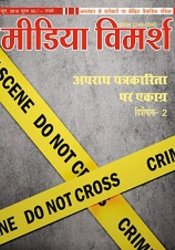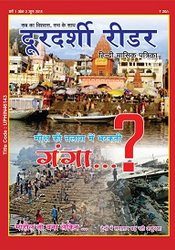मनोज कुमार / भारत के स्वाधीन होने के बाद 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। इसके बाद संविधान के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक पांच वर्ष बाद निर्धारित समय में चुनाव कराये जाने की व्यवस्था की गई। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये जिन संस्थाओं को संविधानवेत्ताओं ने अपनी स्वीकृति सहमति दी उनमें संसद एवं विधानसभाओं के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस को स्थान दिया गया। लोकतंत्र तथा समाज के प्रति प्रेस को जवाबदेह बनाया गया था जिसके पीछे दृष्टि पारदर्शिता की थी क्योंकि प्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो राग-द्वेष से परे रह निरपेक्ष भाव से अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। स्वाधीनता पूर्व के संघर्ष में भारतीय समाज ने प्रेस की भूमिका को देखा और समझा था अत: प्रेस पर विश्वास सहज हो जाता है।
भारत वर्ष में चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही प्रेस का संजीदा हस्तक्षेप रहा है। चुनाव प्रक्रिया निर्बाध रूप से पूर्ण हो, मतदाताओं को सही और उचित जानकारी मिल सके, एक स्वच्छ सरकार का निर्माण हो तथा समय-समय पर प्रेस सरकार को उत्तरादायी बनाने के लिये उसे सजग करता रहे। प्रेस की इस भूमिका को समाज ने स्वीकार किया और प्रेस के माध्यम से मिलने वाली सूचना पर उसका ऐतबार रहा। 1952 के चुनाव के बाद से निरंतर प्रेस का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता गया। प्रेस कई भागों में विभक्त हो गया और एक खास विचारधारा के साथ उसकी भूमिका भी बंट गयी। प्रेस अपने अपने निहित विचारधाराओं के साथ चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों एवं दलों को चिन्हित करने लगे तथा झुकाव भी उनकी ओर दिखने लगा। इन सबके बावजूद चुनाव में प्रेस राष्ट्रीय एकता, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के खिलाफ खड़ा दिखाई देता रहा।
यह वह समय था जब देश में विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत हो रही थी। विकास के साथ आर्थिक अनियमितताओं की खबरें भी आने लगी थी। यह वही समय था जब प्रेस आधुनिक सुविधाओं से लबरेज नहीं था। यह वही समय था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार नहीं हो पाया था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर रेडियो था। इस पर भी सरकारी ठप्पा लगा हुआ था और यह अविश्वसनीय भले ही नहीं था किन्तु विश्वास भी नहीं था। इसका उपयोग समाज केवल सूचना पाने के लिये करता था। यह वही समय था जब समाचार पत्रों का व्यापक प्रभाव एवं प्रसार था। कोई चार पन्ने तो अधिकतम आठ पन्ने के श्वेत-श्याम समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था। प्रेस की एक सीमा था और उसका अपना आत्मनियमन। दुख और दुर्घटना की खबरें संजीदा होकर प्रकाशित की जाती थी। स्वाभाविक है कि जब प्रेस के पास आत्मनियमन होगा तो वह चुनाव में भी अपनी ही लक्ष्मण रेखा को लांघने का दुस्साहस नहीं करेगी।
आत्मनियमन से बंधे प्रेस की यह भूमिका समाज के लिये आदर्श उदाहरण हुआ करती थी। आत्मनियमन और प्रेस की स्वयं की खींची लक्ष्मणरेखा 70 के दशक के आते-आते दरकती हुई दिखायी देने लगी। सन् 75 के आपातकाल के बाद तो जैसे प्रेस का चेहरा एकाएक बदल गया। आत्मनियमन का बंधन खत्म हो गया और लक्ष्मणरेखा को लांघने में प्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ समाचार पत्र सरकार की चाटुकारिता में ऐसे लग गये कि प्रेस पर समाज का विश्वास अविश्वास में बदलने लगा। आपातकाल में सरकार के नियंत्रण एवं हमले ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया। जो प्रेस डरा नहीं, वह खत्म होने के कगार पर आ गये और जिसने प्रलोभन स्वीकार कर लिया, वे चमक गये। इसके अनेक उदाहरण इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं जिन्हें पढ़ा और समझा जा सकता है।
सन् 75 के आपातकाल के बाद प्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा बदलता हुआ दिखाई देता है। आपातकाल के बाद होने वाले चुनाव में सत्ताधीश पार्टी कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चलती है। गैर-कांग्रेसी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाता है और देश में पहली दफा गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हो जाता है। इस गैर-कांग्रेसी सरकार की उम्र बहुत छोटी होती है। आपसी मतभेद और मनभेद में जल्द ही कांग्रेस सरकार की वापसी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रेस भी पक्षकार बन जाता है। यह वही प्रेस है जो सन् 75 के आपातकाल के पहले तक निरपेक्ष था।
सन् 75 के बाद के सालों में टेक्रालॉजी के विकास का क्रम शुरू होता है और इस विकास का लाभ प्रेस को मिलता है। आयतित कागजों पर प्रतिबंध समाप्त नहीं होने के कारण कुछ वजनदार प्रेस ही अच्छे कागज का उपयोग करते हैं तथा अखबारों के पन्नों की संख्या भी बढ़ जाती है। अधिसंख्य अखबार देशी कागज पर ही निर्भर रहते हैं और कागज की कोटा पद्वति के कारण उन्हें सीमित मात्रा में ही कागज उपलब्ध हो पाता है। ऐसे में समाचार पत्र के पन्नों की संख्या बढ़ नहीं पाती है।
प्रेस के लिये यह स्थिति 80 के दशक तक जारी रहती है लेकिन इसके बाद से स्थिति में एकदम से परिवर्तन होता है। 1982 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे सहानुभूति लहर से कांग्रेस की सत्ता में जोरदार वापसी होती है और इसी के साथ प्रेस स्पष्ट रूप से सत्ता समर्थक एवं सत्ता विरोधी के रूप में पहिचाने जाते हैं। स्वाभाविक है कि प्रेस की यह भूमिका और हस्तक्षेप चुनाव में भी होता है। बाद के वर्षों के चुनाव में प्रेस का यह रोल और अधिक प्रभावी हो जाता है।
चुनाव के समय प्रेस को विज्ञापनों के रूप में आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास ही प्राथमिक उद्देश्य होता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अचानक से राजनीति में आने वाले राजीव गांधी ने चुनाव में विज्ञापनों के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। उनके पहले चुनाव प्रचार सामग्री में सामाजिक मुद्दे, विपक्ष या सत्तापक्ष की विफलता आदि-इत्यादि होती थी जिसे बदलकर सांप-बिच्छू जैसे विज्ञापन बनाये गये। भारतीय समाज के पाठकों की मानसिकता एकदम भिन्न होती थी सो उनसे इन विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस को कोई बड़ा लाभ नहीं मिला।
1952 से लेकर 1975 तथा 75 लेकर 90 तक की स्थितियां, चुनाव और प्रेस की भूमिका की समीक्षा करें तो पहले दौर में प्रेस निरपेक्ष होकर राजनीतिक दलों की देश के प्रति प्रतिबद्धता, आम आदमी के हक में किये गये कार्यों एवं दलगत प्रत्याशी की खूबी-खामियों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते थे ताकि मतदाता सक्रिय एवं बेदाग जनप्रतिनिधि को चुन सके। दूसरे दौर में प्रेस की समाज के प्रति यह प्रतिबद्धता कम होती नजर आती है और चुनाव में वह निरपेक्ष नहीं रह पाता है। वह दलगत राजनीति के पक्ष या विपक्ष में खड़ा दिखता है।
90 के दशक में प्रेस मीडिया में परिवर्तित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवतरित होता है। समाचार पत्रों के कलेवर एवं पृष्ठ संख्या में एकाएक वृद्धि होने लगती है। लगभग पूरा का पूरा समाचार पत्र रंगीन हो जाता है। समाचार पत्रों की इस रंगीनियत में प्रेस की लक्ष्मणरेखा स्वयंमेव टूटने लगती है और आत्मनियमन काफूर हो जाता है। दुर्घटना कितनी बड़ी क्यों न हो, अब वह भी रंगीन होती है जैसा कि कोई उत्सव हो। मरने वालों की संख्या को अतिरंजित कर सज्जा कर प्रस्तुत किया जाता है। दरअसल, यह परिवर्तन उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होड़ लेने के लिये बाध्य करने के कारण होता है। इधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नया अनुभव पाठकों से दर्शकों में बदल रहे मतदाताओं को रोमांचित करता है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने आरंभिक दिनों में बेहद संतुलित होता है लेकिन चैनलों के विस्तार और स्वयं को सबसे ज्यादा कामयाब दिखाने की होड़ में संतुलन आहिस्ता आहिस्ता नदारद होने लगता है। कुछ ऐसी खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह दे दी जाती है जिससे फौरीतौर पर तो खबर दिखाने वाले चैनल की जयकारा होती है लेकिन जब हकीकत सामने आता है तो चैनल की भद पिटती है। ऐसे भद पिटने से चैनलों के चरित्र में कोई सुधार नहीं होता है अपितु उन्हें यह भाने लगता है और यह उनका स्थायी चरित्र बन जाता है। समाज को आईना दिखाने की जवाबदारी जिनकी होती है, वे खुद को आईना दिखा रहे होते हैं।
प्रेस और मीडिया की इसी आपाधापी में शुरू होता है पेडन्यूज का खेल। 90 के दशक के बाद से आहिस्ता आहिस्ता पेडन्यूज के मामले उघडऩे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पेडन्यूज इसी दशक से आरंभ हुआ बल्कि हर चुनाव में पेडन्यूज होता रहा है लेकिन कुछ नैतिकता के साथ। पूर्व में जैसा कि उल्लेख किया गया कि आपातकाल के बाद सरकारी नियंत्रण ने प्रेस की कमर तोडऩे का उपक्रम किया तो पेडन्यूज की परम्परा वहीं से डल गयी थी। फर्क इतना था कि तब समाचार पत्रों का प्रकाशन पेडन्यूज के लिये ही नहीं होता था, कुछ प्रतिशत सामाजिक जवाबदारी भी होती थी और ऐसे समाचारों को कतई प्रकाशित नहीं किया जाता था जो समाज के हित के विपरीत हों।
बहरहाल, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चुनाव सर्वे का सिलसिला आरंभ किया। इसे ओपिनियन पोल, एक्जिट पोल आदि-इत्यादि कहा गया। भारतीय समाज के लिये यह नया अनुभव था। यह जान लेना कि इस बार के चुनाव में मतदाता किसे चुन रहे हैं अथवा अपने खराब प्रदर्शन के बाद भी अमुक सत्ताधारी दल सत्ता में वापसी कर रही है। इन सर्वे का सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। एक के बाद एक चैनल सर्वे करने लगे। एक-दूसरे के सर्वे को चुनौती देने लगे। सत्ताधीशों को यह उपक्रम भाने लगा तो अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिये मनपसंद सर्वे कराने लगे। मतदाताओं का इन सर्वे से मोहभंग होने लगा क्योंकि ज्यादतर सर्वे अपने बताये परिणामों पर खरे नहीं उतर सके। वास्तव में पेडन्यूज का यह एक और दूसरा बड़ा रूप है।
सन् 2000 से लेकर 2013 तक के चुनावों में प्रेस की भूमिका की पड़ताल करें तो सहसा यकिन नहीं होता कि यह वही प्रेस है जिसने सीमित साधनों में अंग्रेज शासन को भारत छोडऩे के लिये मजबूर कर दिया था। खैर, देश का चुनाव आयोग चुनाव में निष्पक्षता कायम रखने और प्रेस पर नियंत्रण पाने के लिये अनेक स्तर पर प्रयास कर रहा है। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने जो प्रयास किये थे आज वह प्रयास और सख्ती के साथ किये जा रहे हैं।
प्रेस और मीडिया के बाद समाज में एक नये संचार माध्यम का उदय होता है जिसे न्यू मीडिया या सोशल मीडिया के नाम से पुकारा गया। अपनी आरंभिक अवस्था में होने के बावजूद इस नये संचार माध्यम का वजूद दिखने लगा। युवा वर्ग में इस माध्यम को लेकर जिज्ञासा थी तो राजनीतिक दलों को कम खर्च, कम समय और प्रभावशाली ढंग से युवाओं के बीच पहुंचने का सशक्त माध्यम मिल गया। प्रेस और मीडिया के दुरूपयोग के बाद राजनीतिक दलों ने इस नये संचार माध्यम को भी अपने राजनीतिक लाभ का हथियार बनाना आरंभ किया। इस नये संचार माध्यम के स्वरूप को बिगाडऩे की कोशिश भी हुई। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कम अनुभव और कम समझ रखने वाले भी राजनीतिक दलों में बंटते चले गये और प्रेस तथा मीडिया में जो शालीनता की एक मर्यादा थी, वह इस नये संचार माध्यम में तार-तार होती गयी। कहना न होगा कि यह माध्यम समाज के लिये आने वाले समय में जितना फायदेमंद होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह भी। जरूरी होगा कि इस पर भी नियंत्रण लगे।
चुनाव आयोग की सख्ती से अनाप-शनाप होने वाले चुनावी खर्चों पर लगाम लगती दिखाई दे रही है। प्रेस और मीडिया को विज्ञापनों के जरिये लुभाने की कोशिश करने वाले राजनीतिक दलों को तब और झटका लगा जब आयोग ने रेडियो एवं सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण का फरमान जारी कर दिया। यही नहीं, तमाम विरोधों के बावजूद पहली दफा चुनाव आयोग ने 2013 के पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में 11 नवम्बर से चुनाव परिणाम आते तक 8 दिसम्बर 2013 तक किसी भी तरह के चुनावी सर्वे पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम अनुचित नहीं कहा जा सकता है। आयोग के इस प्रतिबंध पर चर्चा करने से ज्यादा जरूरी है प्रेस और मीडिया का स्वयं का आत्मलोचन। जिस प्रेस और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, जिस प्रेस और मीडिया के कंधे पर शासन और सरकार को सजग रखने की जवाबदारी है, जो स्वयं समाज का आईना है, आज उस पर ही नियंत्रण हो रहा है तो क्यों?
लेखक वरिष्ठ पत्रकार और भोपाल से प्रकाशित “समागम” के संपादक है